हमने इस पोस्ट में हिंदी व्यंजन Hindi Vyanjan , परिभाषा, भेद और वर्गीकरण के बारे में बताया है |
व्यंजन की परिभाषा (Vyanjan Ki Paribhasha)
व्यंजन के रूप में जाना जाने वाला वर्ण एक ध्वनि का उत्पादन करता है जिसमें कोई स्वर नहीं होता है। व्यंजन वर्ण शब्दों के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं और वे उन वर्णों को बताते हैं जो स्वरों के साथ मिलकर शब्दों के रूप में जुड़ते हैं। हिंदी भाषा में अलग-अलग वर्णों के संयोजन से व्यंजन बनते हैं जो शब्दों का निर्माण करते हैं। हिंदी व्यंजन की संख्या 33 है जो कि बिना स्वर के होते हैं।
अन्य शब्दों में, व्यंजन एक वर्ण होता है जो अल्प प्रकार से उच्चारित होता है और जिसमें स्वर का उच्चारण नहीं होता है। हिंदी वर्णमाला में, व्यंजन वर्ण उस वर्णों को कहते हैं जो कि स्वरों के अतिरिक्त होते हैं। इन वर्णों को समुद्र शास्त्र में “कंठ्य” वर्ण भी कहा जाता है।
हिंदी भाषा में, कुल 33 व्यंजन होते हैं, जो कि अलग-अलग माध्यमों से उच्चारित किए जाते हैं और वर्णमाला में उन्हें वर्ण के बाद लगाया जाता है
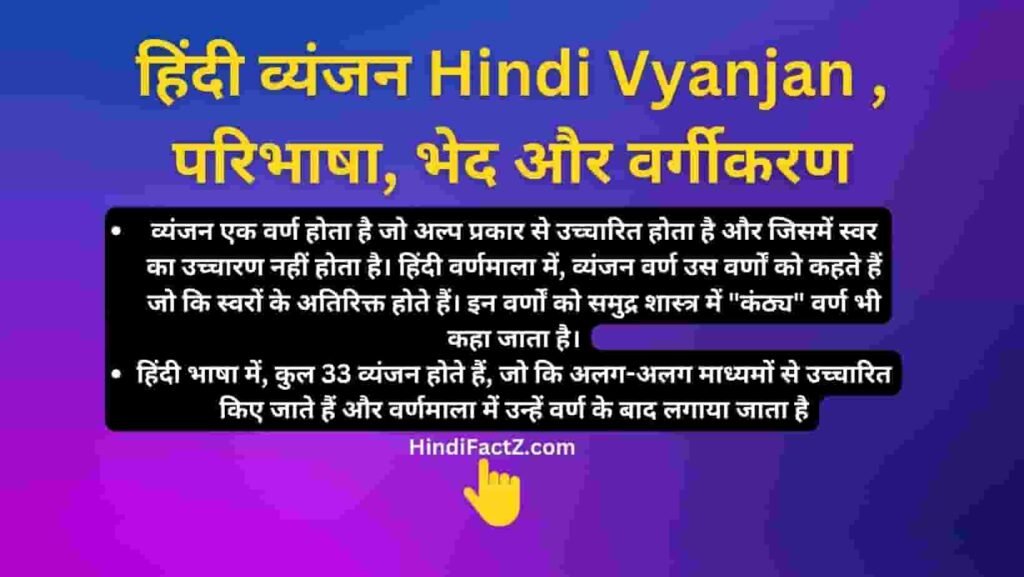
Hindi Vyanjan | हिंदी व्यंजन
हिंदी व्यंजन (Hindi Vyanjan) वर्ण हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत उन वर्णों को कहते हैं जो कि बिना स्वर के होते हैं। हिंदी में कुल 33 व्यंजन होते हैं। निम्नलिखित हैं हिंदी व्यंजनों के नाम और उनकी संज्ञा शब्दें:
क – काक, ख – खरगोश, ग – गज़र, घ – घड़ी ङ – अंग्रेज़ी वर्ण की ‘एन’ की आवाज़, च – चाय, छ – छाता, ज – जंगली सुअर, झ – झींगुर ञ – अंग्रेज़ी वर्ण की ‘य’ की आवाज़, ट – टमाटर, ठ – ठंडा, ड – डमरू, ढ – ढोल ण – अंग्रेज़ी वर्ण की ‘एन’ की नाक से उच्च आवाज़, त – ताज़ा, थ – थंडी, द – दमकल, ध – धरती न – नाग, प – परिंदे, फ – फल, ब – बिल्ली, भ – भैंस म – मछली, य – यक, र – राजा, ल – लड़का, व – वाक्य, श – शेर ष – अंग्रेज़ी वर्ण की ‘श’ की नाक से उच्च आवाज़, स – समुन्द्र, ह – हाथी, क्ष – अंग्रेज़ी वर्ण की ‘श’ और ‘क’ के मेल से हुआ वर्ण, त्र – त्रिकोण, ज्ञ – ज्ञान |
उच्चारण के आधार पर व्यंजन के आठ भेद
हिंदी भाषा में व्यंजन के आठ भेद उच्चारण के आधार पर निम्नलिखित होते हैं:
- प्रकम्पित व्यंजन
- संघर्षी व्यंजन
- उत्क्षिप्त व्यंजन
- स्पर्श संघर्षी व्यंजन
- नासिक्य व्यंजन
- स्पर्श व्यंजन
- संघर्षहीन व्यंजन
- पार्श्विक व्यंजन
प्रकम्पित व्यंजन
प्रकम्पित व्यंजन हमारी ध्वनि उत्पादन प्रक्रिया में बनते हैं। जब हम वाक्य उच्चारित करते हैं, तो हम अपनी आवाज के साथ विभिन्न संकेत और इशारों का उपयोग करते हैं जो कि व्यंजनों के रूप में दिखाई देते हैं।
प्रकम्पित व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिन्हें उच्च दाब के साथ उत्पन्न किया जाता है। ये व्यंजन थोड़े समय तक बाधित होते हैं और फिर उन्हें छोड़ते हुए उच्चारण किया जाता है। हिंदी में कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं:
- क, ख, ग, घ, ङ
- च, छ, ज, झ, ञ
- ट, ठ, ड, ढ, ण
- त, थ, द, ध, न
- प, फ, ब, भ, म
इन सभी व्यंजनों को उच्च दाब द्वारा उत्पन्न किया जाता है जबकि स्पर्श व्यंजनों को उत्पन्न करने के लिए जीभ का उपयोग किया जाता है।
संघर्षी व्यंजन
संघर्षी व्यंजन हमारी ध्वनि उत्पादन प्रक्रिया में उत्पन्न होते हैं। इन व्यंजनों का उत्पादन दो अलग-अलग व्यंजनों के संयोजन या संघर्ष के कारण होता है। हमारे मुख में अलग-अलग व्यंजनों के उत्पादन के लिए अलग-अलग भाग होते हैं और इन व्यंजनों को उत्पन्न करने के लिए इन भागों के संयोजन या संघर्ष करने की आवश्यकता होती है।
हिंदी में कुछ संघर्षी व्यंजन हैं जैसे क्ष, त्र, ज्ञ आदि। इन व्यंजनों का उत्पादन दो व्यंजनों के संयोजन से होता है। उदाहरण के लिए, क्ष व्यंजन का उत्पादन क के व्यंजन और ष व्यंजन के संयोजन से होता है। इन व्यंजनों के उच्चारण के लिए हमें अलग-अलग भागों को संघर्ष करना पड़ता है और उन्हें आसानी से उच्चारित करने के लिए अभ्यास करना पड़ता है।
उत्क्षिप्त व्यंजन
उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं जो उच्च ध्वनियों के उत्पादन में उपयोगी होते हैं। इन व्यंजनों को उच्च उच्चारण या उच्च स्थान से उच्चारित किया जाता है। उदाहरण के लिए, हिंदी में ‘ख’, ‘घ’, ‘छ’, ‘झ’ और ‘ठ’ उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। ये व्यंजन संघर्षी व्यंजनों से अलग होते हैं जो मुख्य रूप से निम्न ध्वनियों के उत्पादन में उपयोगी होते हैं।
स्पर्श संघर्षी व्यंजन
स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं जो दो वर्णों के संघर्ष से उत्पन्न होते हैं और उनके उच्चारण में जीभ, दाँत और होंठों का उपयोग किया जाता है। ये व्यंजन उच्च ध्वनियों के उत्पादन में मददगार होते हैं। हिंदी में ‘क’, ‘ख’, ‘ग’, ‘घ’, ‘च’, ‘छ’, ‘ज’, ‘झ’, ‘ट’, ‘ठ’, ‘ड’, ‘ढ’, ‘त’ और ‘थ’ इस श्रेणी के उदाहरण हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ और दाँतों का संघर्ष होता है और होंठों का उपयोग उन्हें संचारित करने में मदद करता है।
नासिक्य व्यंजन
नासिक्य व्यंजन होते हैं जो नाक के उपरी भाग या नाक के अंदरी भाग का उपयोग करते हुए उत्पन्न होते हैं। हिंदी में ‘म’, ‘न’, ‘ङ’, ‘ञ’ और ‘ण’ इस श्रेणी के उदाहरण हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण में नाक का उपयोग किया जाता है। नाक के उपरी भाग से उत्पन्न होने वाले नासिक्य व्यंजन को अधिकांश भाषाओं में अंग्रेजी में “nasal consonants” या “nasals” कहा जाता है।
स्पर्श व्यंजन
स्पर्श व्यंजन होते हैं जो अपने उत्पत्ति स्थान पर विभिन्न प्रकार के संघर्ष के माध्यम से उत्पन्न होते हैं। हिंदी व्याकरण में, जैसे कि ‘क’, ‘ट’, ‘ग’, ‘ठ’, ‘च’, ‘ड’, ‘ज’ और ‘ढ’ ये सभी स्पर्श व्यंजन हैं। ये व्यंजन उच्चारित करने के लिए जीभ और मुँह के संघर्ष का उपयोग किया जाता है। इन व्यंजनों में, जीभ को पीछे की ओर घुमाया जाता है और मुँह को खोला जाता है ताकि संघर्ष हो सके।
संघर्षहीन व्यंजन
संघर्षहीन व्यंजन होते हैं जो उच्चारित करते समय किसी भी तरह का संघर्ष नहीं करते हैं। इन व्यंजनों को उच्चारित करने के लिए सिर्फ वायु को निःशक्त करना होता है। हिंदी व्याकरण में, जैसे कि ‘प’, ‘फ’, ‘ब’, ‘भ’, ‘त’, ‘थ’, ‘द’, ‘ध’, ‘च’, ‘छ’, ‘ज’ और ‘झ’ ये सभी संघर्षहीन व्यंजन होते हैं। इन व्यंजनों को उच्चारित करने के लिए जीभ को कहीं भी नहीं घुमाया जाता है और मुँह को बिल्कुल नहीं खोलना पड़ता है।
पार्श्विक व्यंजन
पार्श्विक व्यंजन होते हैं जो उच्चारित करते समय जीभ को उँगलियों से टच करते हुए या उनसे पार करते हुए उच्चारित किए जाते हैं। हिंदी भाषा में ‘श’, ‘ष’, ‘स’, ‘ह’, ‘क्ष’ और ‘ज्ञ’ इन सभी व्यंजनों को पार्श्विक व्यंजन के रूप में श्रृंखला में शामिल किया जाता है। इन व्यंजनों को उच्चारित करने के लिए जीभ को उँगलियों से टच करना पड़ता है या उनसे पार करना पड़ता है।
हिंदी व्यंजन का वर्गीकरण
हिंदी व्यंजन (Hindi Vyanjan) को उनके उच्चारण स्थान, स्वर-तन्त्रियों की स्थिति और संघर्ष के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है।
- उच्चारण स्थान के आधार पर:
- मूर्द्धा वर्ग (या शीर्ष वर्ग): क, ख, ग, घ, ङ
- तालु वर्ग: च, छ, ज, झ, ञ
- मूख वर्ग: ट, ठ, ड, ढ, ण
- ओष्ठ्य वर्ग: त, थ, द, ध, न
- दंत्य वर्ग: प, फ, ब, भ, म
- अनुनासिक वर्ग: य, र, ल, व
- अनुस्वार वर्ग: अं, अः
- विसर्ग वर्ग: अँ, ः
- स्वर-तन्त्रियों की स्थिति के आधार पर:
- ह्रस्व स्वर वर्ग: इ, उ, ए, ओ
- दीर्घ स्वर वर्ग: ई, ऊ, ऐ, औ
- संघर्ष के आधार पर:
- संघर्षहीन वर्ग: अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ
- संघर्षी वर्ग: क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ, य, र, ल, व, श, ष, स, ह, क्ष, ज्ञ
इस तरह से हिंदी व्यंजन (Hindi Vyanjan) को वर्गीकृत किया जाता है।
हिंदी व्यंजनों (Hindi Vyanjan) को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है:
- ओसवार वर्ग: क, ख, ग, घ, ङ
- तालव्य संयोजक वर्ग: च, छ, ज, झ, ञ
- मूर्धन्य वर्ग: ट, ठ, ड, ढ, ण
- दंत्य वर्ग: त, थ, द, ध, न
- ओष्ठ्य वर्ग: प, फ, ब, भ, म
- कण्ठ्य वर्ग: य, र, ल, व
- तालव्य वर्ग: श, ष, स, ह
- अनुस्वार और विसर्ग: अनुस्वार (अं) और विसर्ग (अः) भी व्यंजन वर्णों के रूप में माने जाते हैं।
इन वर्गों को याद करने से हम अपनी हिंदी भाषा के व्यंजन वर्णों को आसानी से समझ और सीख सकते हैं।
स्वर तन्त्रियों की स्थितिघोष के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण
हिंदी व्यंजनों (Hindi Vyanjan) का वर्गीकरण स्वर तंत्रियों की स्थिति के आधार पर निम्नलिखित तरीके से किया जा सकता है।
- स्वर – स्वर वह ध्वनि होती है जिसके उच्चारण के दौरान स्वर तंत्रियों की स्थिति निरंतर बदलती रहती है। स्वर के उच्चारण के दौरान जीभ, होंठ और श्वसन नली की स्थिति बदलती रहती है। उदाहरण के लिए, अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ इत्यादि सभी स्वर होते हैं।
- व्यंजन – व्यंजन ध्वनियों में स्वर तंत्रियों की स्थिति नहीं बदलती होती है। इन ध्वनियों को उच्चारित करते समय जीभ और होंठों की स्थिति बदलती है, लेकिन श्वसन नली की स्थिति नहीं बदलती होती है। उदाहरण के लिए, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ष, स, ह इत्यादि सभी व्यंजन होते हैं।
इस तरह से, हिंदी व्यंजनों (Hindi Vyanjan) का वर्गीकरण स्वर तंत्रियों की स्थिति के आधार पर किया जा सकता है।
Other related Posts to Hindi Vyakaran
हिंदी वर्णमाला (Hindi Alphabet Varnamala)
संज्ञा किसे कहते हैं (Sangya kise kahate hain) – परिभाषा, भेद एवं उदाहरण
कारक किसे कहते हैं – परिभाषा एवं कारक चिह्न










